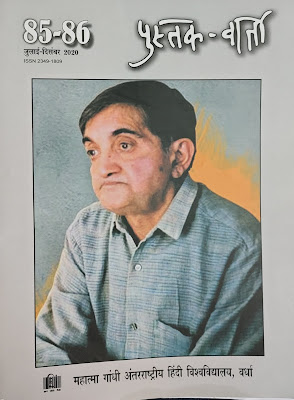जीवन की महायात्रा और ये धरती एक सराय
मृत्यु इस जीवन की सबसे बड़ी पहेली है और साथ ही सबसे बड़ा भय भी, चाहे वह अपनी हो या अपने किसी नजदीकी रिश्ते, सम्बन्धी या आत्मीय परिजन की। ऐसा क्यों है, इसके कई कारण हैं। जिसमें प्रमुख है स्वयं को देह तक सीमित मानना, जिस कारण अपनी देह के नाश व इससे जुड़ी पीड़ा की कल्पना से व्यक्ति भयाक्रांत रहता है। फिर अपने निकट सम्बन्धियों, रिश्तों-नातों, मित्रों के बिछुड़ने व खोने की वेदना-पीड़ा, जिनको हम अपने जीवन का आधार बनाए होते हैं व जिनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। और तीसरा सांसारिक इच्छाएं-कामनाएं-वासनाएं-महत्वाकांक्षाएं, जिनके लिए हम दिन-रात को एक कर अपने ख्वावों का महल खड़ा कर रहे होते हैं, जैसे कि हमें इसी धरती पर हर-हमेशा के लिए रहना है और यही हमारा स्थायी घर है।
लेकिन मृत्यु का नाम सुनते ही, इसकी आहट मिलते ही, इसका साक्षात्कार होते हैं, ये तीनों तार, बुने हुए सपने, अरमानों के महल ताश के पत्तों की ढेरी की भाँति पल भर में धड़ाशयी होते दिखते हैं, एक ही झटके में इन पर बिजली गिरने की दुर्घटना का विल्पवी मंजर सामने आ खडा होता है। एक ही पल में सारे सपने चकानाचूर हो जाते हैं व जीवन शून्य पर आकर खड़ा हो जाता है।
जो भी हो, मृत्यु एक अकाट्य सत्य है, देर सबेर सभी को इससे होकर गुजरना है, किसी को पहले तो किसी को बाद में, सबका नम्बर तय है, बल्कि जन्म लेते ही इसकी उल्टी गिनती शुरु हो चुकी होती है। हर दूसरे व्यक्ति के मौत के साथ इसकी सूचना की घण्टी बजती रहती है, लेकिन मन सोचता है कि दूसरों की ही तो मौत हुई है, हम तो जिंदा है और मौत का यह सिलसिला तो चलता रहता है, मेरी मौत में अभी देर है। यह मन की माया का एक विचित्र खेल है। लेकिन हर व्यक्ति की सांसें निर्धारित हैं, यहाँ तक की मृत्यु का स्थान और तरीका भी। हालाँकि यह बात दूसरी है इस सत्य से अधिकाँश लोग अनभिज्ञ ही रहते हैं। केवल त्रिकालदर्शी दिव्य आत्माएं व सिद्ध पुरुष ही इसके यथार्थ से भिज्ञ रहते हैं।
जब कोई पूरी आयु जीकर संसार छोड़ता है, तो उसमें अधिक गम नहीं होता, क्योंकि सभी इसके लिए पर्याप्त रुप से तैयार होते हैं, विदाई ले रही जीवात्मा भी और उसके परिवार व निकट परिजन भी। लेकिन जब कोई समय से पहले इस दुनियाँ को अल्विदा कह जाता है, या काल का क्रूर शिंकंजा उसको हमसे छीन लेता है या कहें भगवान बुला लेता है, तो फिर एक बज्रपात सा अनुभव होता है, एक भूचाल सा आ जाता है, जिसमें शुरु में कुछ अधिक समझ नहीं आता। व्यक्ति अपनी कॉम्मन सेंस के आधार पर स्थिति को संभालता है, परिस्थिति से निपटता है। ऐसे में अपनों का व शुभचिंतकों का सहयोग-सम्बल मलमह का काम करता है। धीरे-धीरे कुछ सप्ताह, माह बाद व्यक्ति इस शोकाकुल अवस्था से स्वयं को बाहर निकलता हुआ पाता है।
इस तरह काल जख्म को भरने की अचूक औषधि सावित होता है। लेकिन जख्म तो जख्म ही ठहरे। कुरेदने पर, यादों के ताजा होने पर यदा-कदा रुह को कचोटने वाली वेदना के रुप में उभरते रहते हैं, जो हर भुगत भोगी के हिस्से में आते हैं। ऐसे स्थिति में भावुक होना स्वाभाविक है, आंसुओं का झरना स्वाभाविक है, ह्दय में भावों का स्फोट स्वाभाविक है। लेकिन रोते-कलपते ही रहा जाए, शोक ही मनाते रहा जाए, तो इसमें भी समाधान नहीं, किसी भी प्रकार तन-मन व आत्मा के लिए यह हितकर नहीं। इस स्थिति से उबरने के लिए हर धर्म, संस्कृति व समाज में ऐसी सामूहिक व्यवस्था रहती है, कि शोक बंट जाता है व परिवार का मन हल्का होता है। सनातन धर्म में इसके निमित तेरह दिन, एक माह या चालीस दिन तथा इससे आगे तक धार्मिक कर्मकाण्डों का सिलसिला चलता रहता है, जिनका शोक निवारण के संदर्भ में अपना महत्व रहता है। हर वर्ष पितृ-पक्ष में श्राद्ध तर्पण का विधान इसी तरह का एक विशिष्ट प्रयोग रहता है।
इनके साथ अपनी शोक-वेदना को सृजनात्मक मोड़ दिया जाता है। इसमें जीवन-मरण, लोक-परलोक व अध्यात्म से जुड़ी पुस्तकों का परायण बहुत सहायक रहता है। इनसे एक तो सांत्वना मिलती है, दूसरा इनके प्रकाश में जीवन के प्रति एक नई अंतर्दृष्टि व समझ विकसित होती है, जो इस शोकाकुल समय को पार करने में बहुत कारगर रहती हैं।
साथ ही समझ आता है, कि धरती अपना असली घर नहीं, असली घर तो आध्यात्मिक जगत है, जहाँ जीवात्मा देह छोड़ने के बाद वास करती है। हालाँकि इस मृत्युलोक और जीवात्मा जगत के बीच यात्रा का सिलसिला चलता रहता है, जब तक कि जीवात्मा मुक्त न हो जाए। इस प्रक्रिया पर थोडा सा भी गहराई से चिंतन व विचार मंथन जाने-अनजाने में ही व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन की गहराइयों में प्रवेश दिला देता है। और इसके साथ जीवन-मरण, लोक-परलोक, स्वर्ग-नरक, पुनर्जन्म, कर्मफल सिद्धान्त जैसी बातें गहराई में समझ आने लगती हैं। समझ आता है कि जन्म-मरण का सिलसिला न जाने कितना बार घटित हो चुका है और आगे कितनी बार इससे गुजरा शेष है, जब तक कि कर्मों का हिसाब-किताब पूरा न हो जाए।
समझ आता है कि धरती पर जन्म अपने कर्मों के सुधार के लिए होता है, यह धरती एक प्रशिक्षण केंद्र है, कर्मभोग की भूमि है और साथ ही कर्मयोग भूमि भी, जहाँ एक अच्छे एवं श्रेष्ठ जीवन जीते हुए अपना आत्म परिष्कार करते हुए, जीवात्मा जगत में अपने स्तर को उन्नत करना है। संयम-सदाचार से लेकर सेवा साधना आदि के साथ अपने सद्गुणों का विकास करते हुए जीवात्मा अपने कर्म सुधार कर सकती है तथा इनके अनुरुप जीवात्मा जगत में उच्चतर लोकों में स्थान मिलता है।
इन सबके साथ जीवन-मरण का खेल और मृत्यु की अबुझ पहेली के समाधान तार हाथ में आने शुरु हो जाते हैं व धरती पर एक सार्थक जीवन के मायने व अर्थ समझ आते हैं। सांसारिक मोह-माया व अज्ञानता-मूढ़ता की बेहोशी टूटती है व एक नए होश, जोश व समझ के साथ जीवन के क्रियाक्लापों का पुनर्निधारण होता है। इस सबमें ईश्वर या किसी दूसरे को दोषी मानने की भूल से भी बचाव होता है। अंततः अपने कर्मों के ईर्द-गिर्द ही सब केंद्रित समझ आता है - जन्म भी, मृत्यु भी, स्वर्ग भी, नरक भी, पुनर्जन्म भी और अन्ततः मुक्ति भी। इसके साथ ही हर स्तर पर अपनी भूल-चूक, त्रुटियों व गल्तियों के सुधार, अपने दोषों के परिमार्जन व अपने कर्मों के सुधार की प्रक्रिया अधिक प्रगाढ़ रुप में गति पकड़ती है।
इस तरह मृत्यु के सत्य से दीक्षित पथिक इस धरती रुपी सराय का बेहतरतम उपयोग करता है और जब मृत्यु रुपी दूत दस्तक दे जाता है, तो पथिक अपनी अर्जित धर्म-पुण्य और सत्कर्मों की पूँजी के साथ बोरिया-बिस्तर समेटते हुए इस धरती पर एक प्रेरक विरासत छोड़ते हुए महायात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ चलता है।